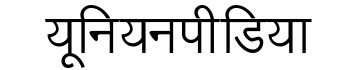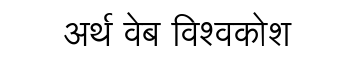सामग्री की तालिका
19 संबंधों: चंपू, तुंगभद्रा नदी, दुर्गसिंह, पञ्चतन्त्र, परमार भोज, प्रतीच्य चालुक्य, मस्की, मान्यखेट, मुद्रा (भाव भंगिमा), रायचूर, शैव, जय सिंह द्वितीय, जयसिंह, जैन धर्म, कन्नड़ भाषा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल, कोल्हापुर, कोंकण, अभिलेख।
- ११वीं शताब्दी के भारतीय शासक
चंपू
चम्पू श्रव्य काव्य का एक भेद है, अर्थात गद्य-पद्य के मिश्रित् काव्य को चम्पू कहते हैं। गद्य तथा पद्य मिश्रित काव्य को "चंपू" कहते हैं। काव्य की इस विधा का उल्लेख साहित्यशास्त्र के प्राचीन आचार्यों- भामह, दण्डी, वामन आदि ने नहीं किया है। यों गद्य पद्यमय शैली का प्रयोग वैदिक साहित्य, बौद्ध जातक, जातकमाला आदि अति प्राचीन साहित्य में भी मिलता है। चम्पूकाव्य परंपरा का प्रारम्भ हमें अथर्व वेद से प्राप्त होता है। चम्पू नाम के प्रकृत काव्य की रचना दसवीं शती के पहले नहीं हुई। त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित 'नलचम्पू', जो दसवीं सदी के प्रारम्भ की रचना है, चम्पू का प्रसिद्ध उदाहरण है। इसके अतिरिक्त सोमदेव सुरि द्वारा रचित यशःतिलक, भोजराज कृत चम्पू रामायण, कवि कर्णपूरि कृत आनन्दवृन्दावन, गोपाल चम्पू (जीव गोस्वामी), नीलकण्ठ चम्पू (नीलकण्ठ दीक्षित) और चम्पू भारत (अनन्त कवि) दसवीं से सत्रहवीं शती तक के उदाहरण हैं। यह काव्य रूप अधिक लोकप्रिय न हो सका और न ही काव्यशास्त्र में उसकी विशेष मान्यता हुई। हिन्दी में यशोधरा (मैथिलीशरण गुप्त) को चम्पू-काव्य कहा जाता है, क्योंकि उसमें गद्य-पद्य दोनों का प्रयोग हुआ है। गद्य और पद्य के इस मिश्रण का उचित विभाजन यह प्रतीत होता है कि भावात्मक विषयों का वर्णन पद्य के द्वारा तथा वर्णनात्मक विषयों का विवरण गद्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाय। परन्तु चंपूरचयिताओं ने इस मनोवैज्ञानिक वैशिष्ट्य पर विशेष ध्यान न देकर दोनों के संमिश्रण में अपनी स्वतंत्र इच्छा तथा वैयक्तिक अभिरुचि को ही महत्व दिया है। .
देखें जयसिंह द्वितीय (पश्चिमी चालुक्य) और चंपू
तुंगभद्रा नदी
तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत में बहने वाली एक पवित्र नदी हैं। यह कर्नाटक एवं आन्ध्र प्रदेश में बहती हुई आन्ध्र प्रदेश में एक बड़ी नदी कृष्णा नदी में मिल जाती है। रामायण में तुंगभद्रा को पंपा के नाम से जाना जाता था। तुंगभद्रा नदी का जन्म तुंगा एवं भद्रा नदियों के मिलन से हुआ है। ये पश्चिमी घाट के पूर्वा ढाल से होकर बहती है। पश्चिमी घाट के गंगामूला नामक स्थान से (उडुपी के पास) समुद्र तल से कोई ११९८ मीटर की ऊँचाई से तुंग तथा भद्रा नदियों का जन्म होता है जो शिमोगा के पास जाकर सम्मिलित होती हैं जहाँ से इसे तुंगभद्रा कहते हैं। उत्तर-पूर्व की ओर बहती हुई, आंध्रप्रदेश में महबूब नगर ज़िले में गोंडिमल्ला में जाकर ये कृष्णा नदी से मिल जाती है। इसके किनारों पर कई हिंदू धार्मिक स्थान हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित शृंगेरी मठ तुंगा नदी के बांई तट पर बना है और इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है। चौदहवीं सदी में स्थापित दक्कनी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही हंपी भी इसी के किनारे स्थित है। हंपी में बहती तुंगभद्रा नदी हम्पी के निकट तुंग नदी एवं भद्रा नदी के संगम से तुंगभद्रा नदी का उद्गम होता है। .
देखें जयसिंह द्वितीय (पश्चिमी चालुक्य) और तुंगभद्रा नदी
दुर्गसिंह
दुर्गसिंह (काल: १०२५ ई) चालुक्य नरेश जयसिंह द्वितीय के 'संधि-विग्रह' के मंत्री थे। उन्होने संस्कृत में उपलब्ध पंचतंत्र की कहानियों का कन्नड में अनुवाद किया जिसमें 'चंपू' छन्द का प्रयोग हुआ है। इसमें कुल ६० कथाएँ हैं जिनका झुकाव जैन धर्म की तरफ है। इनमें से १३ कहानियाँ मौलिक हैं। प्रत्येक कथा के अन्त में 'कथाश्लोक' है जिसमें उस कथा का सारांश एवं शिक्षा दी गयी है। यह ग्रंथ पंचतंत्र का भारतीय लोकभाषाओं में हुए सबसे पहले अनुवादों में से है। श्रेणी:कन्नड कवि श्रेणी:कर्नाटक का इतिहास.
देखें जयसिंह द्वितीय (पश्चिमी चालुक्य) और दुर्गसिंह
पञ्चतन्त्र
'''पंचतन्त्र''' का विश्व में प्रसार संस्कृत नीतिकथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। यद्यपि यह पुस्तक अपने मूल रूप में नहीं रह गयी है, फिर भी उपलब्ध अनुवादों के आधार पर इसकी रचना तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आस- पास निर्धारित की गई है। इस ग्रंथ के रचयिता पं॰ विष्णु शर्मा है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जब इस ग्रंथ की रचना पूरी हुई, तब उनकी उम्र लगभग ८० वर्ष थी। पंचतंत्र को पाँच तंत्रों (भागों) में बाँटा गया है.
देखें जयसिंह द्वितीय (पश्चिमी चालुक्य) और पञ्चतन्त्र
परमार भोज
राजा भोज की प्रतिमा (भोपाल) भोज पंवार या परमार वंश के नवें राजा थे। परमार वंशीय राजाओं ने मालवा की राजधानी धारानगरी (धार) से आठवीं शताब्दी से लेकर चौदहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज्य किया था। भोज ने बहुत से युद्ध किए और अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की जिससे सिद्ध होता है कि उनमें असाधारण योग्यता थी। यद्यपि उनके जीवन का अधिकांश युद्धक्षेत्र में बीता तथापि उन्होंने अपने राज्य की उन्नति में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न होने दी। उन्होंने मालवा के नगरों व ग्रामों में बहुत से मंदिर बनवाए, यद्यपि उनमें से अब बहुत कम का पता चलता है। कहा जाता है कि वर्तमान मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल को राजा भोज ने ही बसाया था, तब उसका नाम भोजपाल नगर था, जो कि कालान्तर में भूपाल और फिर भोपाल हो गया। राजा भोज ने भोजपाल नगर के पास ही एक समुद्र के समान विशाल तालाब का निर्माण कराया था, जो पूर्व और दक्षिण में भोजपुर के विशाल शिव मंदिर तक जाता था। आज भी भोजपुर जाते समय, रास्ते में शिवमंदिर के पास उस तालाब की पत्थरों की बनी विशाल पाल दिखती है। उस समय उस तालाब का पानी बहुत पवित्र और बीमारियों को ठीक करने वाला माना जाता था। कहा जाता है कि राजा भोज को चर्म रोग हो गया था तब किसी ऋषि या वैद्य ने उन्हें इस तालाब के पानी में स्नान करने और उसे पीने की सलाह दी थी जिससे उनका चर्मरोग ठीक हो गया था। उस विशाल तालाब के पानी से शिवमंदिर में स्थापित विशाल शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता था। राजा भोज स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे और कहा जाता है कि उन्होंने धर्म, खगोल विद्या, कला, कोशरचना, भवननिर्माण, काव्य, औषधशास्त्र आदि विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं जो अब भी विद्यमान हैं। इनके समय में कवियों को राज्य से आश्रय मिला था। उन्होने सन् 1000 ई.
देखें जयसिंह द्वितीय (पश्चिमी चालुक्य) और परमार भोज
प्रतीच्य चालुक्य
प्रतीच्य चालुक्य पश्चिमी भारत का राजवंश था जिसने २१६ वर्ष राज किया। प्रतीच्य चालुक्य, c. 1121.
देखें जयसिंह द्वितीय (पश्चिमी चालुक्य) और प्रतीच्य चालुक्य
मस्की
मस्की कर्नाटक के रायचूर जिला का एक ग्राम है। यहाम पुरातात्त्विक स्थल भि है।Amalananda Ghosh (1990), p282 यह मस्की नदी के तट पर स्थित है। यह नदी तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है। यहां १९१५ में सम्राट अशोक महान के शिलालेख प्राप्त हुए थे।V.
देखें जयसिंह द्वितीय (पश्चिमी चालुक्य) और मस्की
मान्यखेट
मान्यखेट (प्राकृत: मन्नखेड़ा, आधुनिक मळखेड) कर्नाटक के गुलबर्ग जिले के सेदम तालुका में कगिना नदी के किनारे स्थित है। यह नगर ८१८ से ९८२ ई तक राष्ट्रकूट राजाओं की राजधानी था। .
देखें जयसिंह द्वितीय (पश्चिमी चालुक्य) और मान्यखेट
मुद्रा (भाव भंगिमा)
---- एक मुद्रा (संस्कृत: मुद्रा, (अंग्रेजी में: "seal", "mark," या "gesture")) हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में एक प्रतीकात्मक या आनुष्ठानिक भाव या भाव-भंगिमा है। जबकि कुछ मुद्राओं में पूरा शरीर शामिल रहता है, लेकिन ज्यादातर मुद्राएं हाथों और उंगलियों से की जाती हैं। एक मुद्रा एक आध्यात्मिक भाव-भंगिमा है और भारतीय धर्म तथा धर्म और ताओवाद की परंपराओं के प्रतिमा शास्त्र व आध्यात्मिक कर्म में नियोजित प्रामाणिकता की एक ऊर्जावान छाप है। नियमित तांत्रिक अनुष्ठानों में एक सौ आठ मुद्राओं का प्रयोग होता है। योग में, आम तौर पर जब वज्रासन की मुद्रा में बैठा जाता है, तब सांस के साथ शामिल शरीर के विभिन्न भागों को संतुलित रखने के लिए और शरीर में प्राण के प्रवाह को प्रभावित करने के लिए मुद्राओं का प्रयोग प्राणायाम (सांस लेने के योगिक व्यायाम) के संयोजन के साथ किया जाता है। नवंबर 2009 में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में प्रकाशित एक शोध आलेख में दिखाया गया है कि हाथ की मुद्राएं मस्तिष्क के उसी क्षेत्र को उत्तेजित या प्रोत्साहित करती हैं जो भाषा की हैं। .
देखें जयसिंह द्वितीय (पश्चिमी चालुक्य) और मुद्रा (भाव भंगिमा)
रायचूर
रायचूर कर्नाटक प्रान्त का एक शहर है। श्रेणी:कर्नाटक श्रेणी:कर्नाटक के शहर.
देखें जयसिंह द्वितीय (पश्चिमी चालुक्य) और रायचूर
शैव
भगवान शिव तथा उनके अवतारों को मानने वालों को शैव कहते हैं। शैव में शाक्त, नाथ, दसनामी, नाग आदि उप संप्रदाय हैं। महाभारत में माहेश्वरों (शैव) के चार सम्प्रदाय बतलाए गए हैं: (i) शैव (ii) पाशुपत (iii) कालदमन (iv) कापालिक। शैवमत का मूलरूप ॠग्वेद में रुद्र की आराधना में हैं। 12 रुद्रों में प्रमुख रुद्र ही आगे चलकर शिव, शंकर, भोलेनाथ और महादेव कहलाए। शैव धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और तथ्य: (1) भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैवधर्म कहा जाता है। (2) शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। (3) ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। (4) अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा जाता है। (5) लिंगपूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्यपुराण में मिलता है। (6) महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। (7) वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या चार बताई गई है: (i) पाशुपत (ii) काल्पलिक (iii) कालमुख (iv) लिंगायत (7) पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लवकुलीश थे जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। (8) पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया, इस मत का सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। (9) कापलिक संप्रदाय के ईष्ट देव भैरव थे, इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र शैल नामक स्थान था। (10) कालामुख संप्रदाय के अनुयायिओं को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग नर-पकाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते थे और शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। (11) लिंगायत समुदाय दक्षिण में काफी प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता है, इस संप्रदाय के लोग शिव लिंग की उपासना करते थे। (12) बसव पुराण में लिंगायत समुदाय के प्रवर्तक वल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बासव को बताया गया है, इस संप्रदाय को वीरशिव संप्रदाय भी कहा जाता था। (13) दसवीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की, इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। (14) दक्षिण भारत में शैवधर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय रहा। (15) नायनारों संतों की संख्या 63 बताई गई है। जिनमें उप्पार, तिरूज्ञान, संबंदर और सुंदर मूर्ति के नाम उल्लेखनीय है। (16) पल्लवकाल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों ने किया। (17) ऐलेरा के कैलाश मदिंर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। (18) चोल शालक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। (19) कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिंव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। (20) शिव पुराण में शिव के दशावतारों के अलावा अन्य का वर्णन मिलता है। ये दसों अवतार तंत्रशास्त्र से संबंधित हैं: (i) महाकाल (ii) तारा (iii) भुवनेश (iv) षोडश (v) भैरव (vi) छिन्नमस्तक गिरिजा (vii) धूम्रवान (viii) बगलामुखी (ix) मातंग (x) कमल (21) शिव के अन्य ग्यारह अवतार हैं: (i) कपाली (ii) पिंगल (iii) भीम (iv) विरुपाक्ष (v) विलोहित (vi) शास्ता (vii) अजपाद (viii) आपिर्बुध्य (ix) शम्भ (x) चण्ड (xi) भव (22) शैव ग्रंथ इस प्रकार हैं: (i) श्वेताश्वतरा उपनिषद (ii) शिव पुराण (iii) आगम ग्रंथ (iv) तिरुमुराई (23) शैव तीर्थ इस प्रकार हैं: (i) बनारस (ii) केदारनाथ (iii) सोमनाथ (iv) रामेश्वरम (v) चिदम्बरम (vi) अमरनाथ (vii) कैलाश मानसरोवर (24) शैव सम्प्रदाय के संस्कार इस प्रकार हैं: (i) शैव संप्रदाय के लोग एकेश्वरवादी होते हैं। (ii) इसके संन्यासी जटा रखते हैं। (iii) इसमें सिर तो मुंडाते हैं, लेकिन चोटी नहीं रखते। (iv) इनके अनुष्ठान रात्रि में होते हैं। (v) इनके अपने तांत्रिक मंत्र होते हैं। (vi) यह निर्वस्त्र भी रहते हैं, भगवा वस्त्र भी पहनते हैं और हाथ में कमंडल, चिमटा रखकर धूनी भी रमाते हैं। (vii) शैव चंद्र पर आधारित व्रत उपवास करते हैं। (viii) शैव संप्रदाय में समाधि देने की परंपरा है। (ix) शैव मंदिर को शिवालय कहते हैं जहां सिर्फ शिवलिंग होता है। (x) यह भभूति तीलक आड़ा लगाते हैं। (25) शैव साधुओं को नाथ, अघोरी, अवधूत, बाबा,औघड़, योगी, सिद्ध कहा जाता है। .
देखें जयसिंह द्वितीय (पश्चिमी चालुक्य) और शैव
जय सिंह द्वितीय
सवाई जयसिंह या द्वितीय जयसिंह (०३ नवम्बर १६८८ - २१ सितम्बर १७४३) अठारहवीं सदी में भारत में राजस्थान प्रान्त के नगर/राज्य आमेर के कछवाहा वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक थे। सन १७२७ में आमेर से दक्षिण छः मील दूर एक बेहद सुन्दर, सुव्यवस्थित, सुविधापूर्ण और शिल्पशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर आकल्पित नया शहर 'सवाई जयनगर', जयपुर बसाने वाले नगर-नियोजक के बतौर उनकी ख्याति भारतीय-इतिहास में अमर है। काशी, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और जयपुर में, अतुलनीय और अपने समय की सर्वाधिक सटीक गणनाओं के लिए जानी गयी वेधशालाओं के निर्माता, सवाई जयसिह एक नीति-कुशल महाराजा और वीर सेनापति ही नहीं, जाने-माने खगोल वैज्ञानिक और विद्याव्यसनी विद्वान भी थे। उनका संस्कृत, मराठी, तुर्की, फ़ारसी, अरबी, आदि कई भाषाओं पर गंभीर अधिकार था। भारतीय ग्रंथों के अलावा गणित, रेखागणित, खगोल और ज्योतिष में उन्होंने अनेकानेक विदेशी ग्रंथों में वर्णित वैज्ञानिक पद्धतियों का विधिपूर्वक अध्ययन किया था और स्वयं परीक्षण के बाद, कुछ को अपनाया भी था। देश-विदेश से उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों और खगोलशास्त्र के विषय-विशेषज्ञों को जयपुर बुलाया, सम्मानित किया और यहाँ सम्मान दे कर बसाया। .
देखें जयसिंह द्वितीय (पश्चिमी चालुक्य) और जय सिंह द्वितीय
जयसिंह
जय सिंह नाम के व्यक्ति.
देखें जयसिंह द्वितीय (पश्चिमी चालुक्य) और जयसिंह
जैन धर्म
जैन ध्वज जैन धर्म भारत के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। 'जैन धर्म' का अर्थ है - 'जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म'। जो 'जिन' के अनुयायी हों उन्हें 'जैन' कहते हैं। 'जिन' शब्द बना है 'जि' धातु से। 'जि' माने - जीतना। 'जिन' माने जीतने वाला। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, अपनी वाणी को जीत लिया और अपनी काया को जीत लिया और विशिष्ट ज्ञान को पाकर सर्वज्ञ या पूर्णज्ञान प्राप्त किया उन आप्त पुरुष को जिनेश्वर या 'जिन' कहा जाता है'। जैन धर्म अर्थात 'जिन' भगवान् का धर्म। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धान्त है। जैन दर्शन में सृष्टिकर्ता कण कण स्वतंत्र है इस सॄष्टि का या किसी जीव का कोई कर्ता धर्ता नही है।सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते है।जैन धर्म के ईश्वर कर्ता नही भोगता नही वो तो जो है सो है।जैन धर्म मे ईश्वरसृष्टिकर्ता इश्वर को स्थान नहीं दिया गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार इस काल के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ द्वारा जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता करने वाले अनेक उल्लेख अ-जैन साहित्य और विशेषकर वैदिक साहित्य में प्रचुर मात्रा में हैं। .
देखें जयसिंह द्वितीय (पश्चिमी चालुक्य) और जैन धर्म
कन्नड़ भाषा
कन्नड़ (ಕನ್ನಡ) भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जानेवाली भाषा तथा कर्नाटक की राजभाषा है। यह भारत की उन २२ भाषाओं में से एक है जो भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में साम्मिलित हैं। name.
देखें जयसिंह द्वितीय (पश्चिमी चालुक्य) और कन्नड़ भाषा
कल्याणी, पश्चिम बंगाल
कल्याणी, पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया ज़िले का एक शहर है। यह कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण के अधीन आता है। .
देखें जयसिंह द्वितीय (पश्चिमी चालुक्य) और कल्याणी, पश्चिम बंगाल
कोल्हापुर
thumb कोल्हापुर महाराष्ट्र प्रान्त का एक शहर है। मुंबई से 400 किलोमीटर दूर कोल्हापुर महाराष्ट्र का एक जिला है। मुंबई से पास होने के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक सप्ताहंत में यहां आते हैं। यह स्थान ऐतिहासिक तथा धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कोल्हापुर का मराठी कला के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विशेष रूप से कोल्हापुरी हस्तशिल्प बहुत प्रसिद्ध है। कोल्हापुरी चप्पलें तो देश विदेश में मशहूर हैं ही। प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और आध्यात्म से रूबरू कराता कोल्हापुर सभी आयु के लोगों को कुछ न कुछ अवश्य देता है। .
देखें जयसिंह द्वितीय (पश्चिमी चालुक्य) और कोल्हापुर
कोंकण
कोंकण अथवा कोंकण तट, भारत के पश्चिमी तट का पर्वतीय अनुभाग हैं। यह ७२० कि.मी लंबा समुद्र तट है। कोंकण में महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते है। प्राचीन काल का सप्त-कोंकण वर्तमान के कोंकण से ज्यादा बड़ा है; इसका उल्लेख सह्याद्री खंड में किया गया है जिसमें उसे परशुराम क्षेत्र कहा गया है। .
देखें जयसिंह द्वितीय (पश्चिमी चालुक्य) और कोंकण
अभिलेख
कंधार स्थित सम्राट अशोक के द्वारा उत्कीर्ण एक पाषाण अभिलेख अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किये गये पाठन सामाग्री को कहते है। प्राचीन काल से इसका उपयोग हो रहा है। शासको के द्वारा अपने आदेशो को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हे देख सके एवं पढ़ सके और पालन कर सके। आधुनिक युग मे भी इसका उपयोग हो रहा है। .
देखें जयसिंह द्वितीय (पश्चिमी चालुक्य) और अभिलेख
यह भी देखें
११वीं शताब्दी के भारतीय शासक
- अधिराजेन्द्र चोल
- अनंगपाल तोमर
- अनहिल्ल
- अश्वपाल
- अहिल
- कुलोत्तुंग चोल प्रथम
- गांगेयदेव
- छित्तराज
- जयसिंह द्वितीय (पश्चिमी चालुक्य)
- जेन्द्र राज
- जोजल देव
- नृप काम २
- परमार भोज
- पृथ्वीपाल
- बाल प्रसाद
- भीमदेव प्रथम
- महिन्दु
- राजाराज चोल १
- राजेन्द्र चोल २
- लक्ष्मीकर्ण
- विक्रमादित्य ५
- विक्रमादित्य ६
- विद्याधर (चन्देल)
- वीरराजेन्द्र चोल
- सत्यश्रय
- होयसल विनयादित्य
जयसिम्हा २, जगदेकमल्ल प्रथम के रूप में भी जाना जाता है।