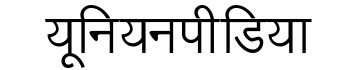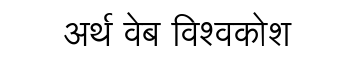सामग्री की तालिका
22 संबंधों: चीकू, नारियल, पपीता, पुष्प, फल, बड़हल, बेर, बीज, लीची, शरीफा, शहतूत, संतरा (फल), जामुन, गूलर, आँवला, आम, इमली, कटहल, केला, अमरूद, अंगूर, उद्यान विज्ञान।
- खाद्य फल
- फल उत्पादन
- वृक्ष
चीकू
चीकू का वृक्ष जिस पर फल लगे हैं। मैसूर में एक स्त्री पके चीकू बेच रही है। चीकू (वानस्पतिक नाम: Manilkara zapota) फल का एक प्रकार हैं। चीकू मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं।.
देखें फलदार वृक्ष और चीकू
नारियल
नारियल के पेड़ नारियल (Cocos nucifera, कोकोस् नूकीफ़ेरा) एक बहुवर्षी एवं एकबीजपत्री पौधा है। इसका तना लम्बा तथा शाखा रहित होता है। मुख्य तने के ऊपरी सिरे पर लम्बी पत्तियों का मुकुट होता है। ये वृक्ष समुद्र के किनारे या नमकीन जगह पर पाये जाते हैं। इसके फल हिन्दुओं के धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त होता है। बांग्ला में इसे नारिकेल कहते हैं। नारियल के वृक्ष भारत में प्रमुख रूप से केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में खूब उगते हैं। महाराष्ट्र में मुंबई तथा तटीय क्षेत्रों व गोआ में भी इसकी उपज होती है। नारियल एक बेहद उपयोगी फल है। नारियल देर से पचने वाला, मूत्राशय शोधक, ग्राही, पुष्टिकारक, बलवर्धक, रक्तविकार नाशक, दाहशामक तथा वात-पित्त नाशक है। .
देखें फलदार वृक्ष और नारियल
पपीता
पपीते के पके फल अन्य पौधों के साथ पपीते का फल लगा पेड़ पपीता एक फल है। कच्ची अवस्था में यह हरे रंग का होता है और पकने पर पीले रंग का हो जाता है। इसके कच्चे और पके फल दोनों ही उपयोग में आते हैं। कच्चे फलों की सब्जी बनती है। इन कारणों से घर के पास लगाने के लिये यह बहुत उत्तम फल है। इसके कच्चे फलों से दूध भी निकाला जाता है, जिससे पपेइन तैयार किया जाता है। पपेइन से पाचन संबंधी औषधियाँ बनाई जाती हैं पपीता पाचन शक्ति को बढ़ाता है। अत: इसके पक्के फल का सेवन उदरविकार में लाभदायक होता है। पपीता सभी उष्ण समशीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में होता है। .
देखें फलदार वृक्ष और पपीता
पुष्प
flower bouquet) पर चित्रकारी रेशम पर स्याही और रंग, १२ वीं शताब्दी की अंत-अंत में और १३ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में. पुष्प, अथवा फूल, जनन संरचना है जो पौधों में पाए जाते हैं। ये (मेग्नोलियोफाईटा प्रकार के पौधों में पाए जाते हैं, जिसे एग्नियो शुक्राणु भी कहा जाता है। एक फूल की जैविक क्रिया यह है कि वह पुरूष शुक्राणु और मादा बीजाणु के संघ के लिए मध्यस्तता करे। प्रक्रिया परागन से शुरू होती है, जिसका अनुसरण गर्भधारण से होता है, जो की बीज के निर्माण और विखराव/ विसर्जन में ख़त्म होता है। बड़े पौधों के लिए, बीज अगली पुश्त के मूल रूप में सेवा करते हैं, जिनसे एक प्रकार की विशेष प्रजाति दुसरे भूभागों में विसर्जित होती हैं। एक पौधे पर फूलों के जमाव को पुष्पण (inflorescence) कहा जाता है। फूल-पौधों के प्रजनन अवयव के साथ-साथ, फूलों को इंसानों/मनुष्यों ने सराहा है और इस्तेमाल भी किया है, खासकर अपने माहोल को सजाने के लिए और खाद्य के स्रोत के रूप में भी। .
देखें फलदार वृक्ष और पुष्प
फल
फल और सब्ज़ियाँ निषेचित, परिवर्तित एवं परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। साधारणतः फल का निर्माण फूल के द्वारा होता है। फूल का स्त्री जननकोष अंडाशय निषेचन की प्रक्रिया द्वारा रूपान्तरित होकर फल का निर्माण करता है। कई पादप प्रजातियों में, फल के अंतर्गत पक्व अंडाशय के अतिरिक्त आसपास के ऊतक भी आते है। फल वह माध्यम है जिसके द्वारा पुष्पीय पादप अपने बीजों का प्रसार करते हैं, हालांकि सभी बीज फलों से नहीं आते। किसी एक परिभाषा द्वारा पादपों के फलों के बीच में पायी जाने वाली भारी विविधता की व्याख्या नहीं की जा सकती है। छद्मफल (झूठा फल, सहायक फल) जैसा शब्द, अंजीर जैसे फलों या उन पादप संरचनाओं के लिए प्रयुक्त होता है जो फल जैसे दिखते तो है पर मूलत: उनकी उत्पप्ति किसी पुष्प या पुष्पों से नहीं होती। कुछ अनावृतबीजी, जैसे कि यूउ के मांसल बीजचोल फल सदृश होते है जबकि कुछ जुनिपरों के मांसल शंकु बेरी जैसे दिखते है। फल शब्द गलत रूप से कई शंकुधारी वृक्षों के बीज-युक्त मादा शंकुओं के लिए भी होता है। .
देखें फलदार वृक्ष और फल
बड़हल
बड़हल (Artocarpus lakoocha या Monkey jack) एक फलदार वृक्ष है। इसका वृक्ष १०-१५ मीटर ऊँचा होता है। इसकी पत्तियाँ २५-३० सेमी लम्बी एवं १५-२० सेमी चौड़ी होती हैं। इसके फल गोल आकार के या बेडौल होते हैं। हरे रंग का कच्चा फल पकने पर पीला हो जाता है जिसे खाया जाता है। इसके अन्दर छोटे-छोटे कोए (जैसे कटहल में) होते हैं। फल का आकार २ से पाँच इंच का होता है। .
देखें फलदार वृक्ष और बड़हल
बेर
डाली में लगा हुआ बेर का फल पके हुए बेर बेर (वानस्पतिक नाम: Ziziphus mauritiana) फल का एक प्रकार हैं। कच्चे फल हरे रंग के होते हैं। पकने पर थोड़ा लाल या लाल-हरे रंग के हो जाते हैं। बेर एक ऐसा फलदार पेड़़ है जो कि एक बार पूरक सिंचाई से स्थापित होने के पश्चात वर्षा के पानी पर निर्भर रहकर भी फलोत्पादन कर सकता है। यह एक बहुवर्षीय व बहुउपयोगी फलदार पेड़ है जिसमें फलों के अतिरिक्त पेड़ के अन्य भागों का भी आर्थिक महत्व है। शुष्क क्षेत्रों में बार-बार अकाल की स्थिति से निपटने के लिए भी बेर की बागवानी अति उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसकी पत्तियाँ पशुओं के लिए पौष्टिक चारा प्रदान करती है जबकि इसमें प्रतिवर्ष अनिवार्य रूप से की जाने वाली कटाई-छंटाई से प्राप्त कांटेदार झाड़ियां खेतों व ढ़ाणियों की रक्षात्मक बाड़ बनाने व भण्डारित चारे की सुरक्षा के लिए उपयोगी है। बेर खेती ऊष्ण व उपोष्ण जलवायु में आसानी से की जा सकती है क्योंकि इसमें कम पानी व सूखे से लड़ने की विशेष क्षमता होती है बेर में वानस्पतिक बढ़वार वर्षा ऋतु के दौरान व फूल वर्षा ऋतु के आखिर में आते है तथा फल वर्षा की भूमिगत नमी के कम होने तथा तापमान बढ़ने से पहले ही पक जाते है। गर्मियों में पौधे सुषुप्तावस्था में प्रवेश कर जाते है व उस समय पत्तियाँ अपने आप ही झड़ जाती है तब पानी की आवश्यकता नहीं के बराबर होती है। इस तरह बेर अधिक तापमान तो सहन कर लेता है लेकिन शीत ऋतु में पड़ने वाले पाले के प्रति अति संवेदनशील होता है। अतः ऐसे क्षेत्रों में जहां नियमित रूप से पाला पड़ने की सम्भावना रहती है, इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। जहां तक मिट्टी का सवाल है, बलुई दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश की मात्रा अधिक हो इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, हालाकि बलुई मिट्टी में भी समुचित मात्रा में देशी खाद का उपयोग करके इसकी खेती की जा सकती है। हल्की क्षारीय व हल्की लवणीय भूमि में भी इसको लगा सकते है। बेर में 300 से भी अधिक किस्में विकसित की जा चुकी है परन्तु सभी किस्में बारानी क्षेत्रों में विशेषकर कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे क्षेत्रों के लिए अगेती व मध्यम अवधि में पकने वाली किस्में ज्यादा उपयुक्त पाई गई है। .
देखें फलदार वृक्ष और बेर
बीज
विभिन्न पौधों के बीज बीज की परिभाषा बीज एक परिपक्व बीजाण्ड है,जो निषेचन के बाद क्रियाशिल होता है,बीज उचित परिस्थितिया जैसे जल,वायु,सूर्य प्रकास आदि मिलने पर क्रियाशिल होता है। .
देखें फलदार वृक्ष और बीज
लीची
लीची एक फल के रूप में जाना जाता है, जिसे वैज्ञानिक नाम (Litchi chinensis) से बुलाते हैं, जीनस लीची का एकमात्र सदस्य है। इसका परिवार है सोपबैरी। यह ऊष्णकटिबन्धीय फल है, जिसका मूल निवास चीन है। यह सामान्यतः मैडागास्कर, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दक्षिण ताइवान, उत्तरी वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका में पायी जाती है। सैमसिंग के फूल, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, भारत इसका मध्यम ऊंचाई का सदाबहार पेड़ होता है, जो कि 15-20 मीटर तक होता है, ऑल्टर्नेट पाइनेट पत्तियां, लगभग 15-25 सें.मी.
देखें फलदार वृक्ष और लीची
शरीफा
शरीफा शरीफा शरीफा या सीताफल (कस्टर्ड ऐपल) एक प्रकार का फल है। इसका वानस्पतिक नाम अन्नोना स्क्वामोसा है। .
देखें फलदार वृक्ष और शरीफा
शहतूत
शहतूत की डाली, पत्तियाँ एवं फल शहतूत की पत्ती पर रखे शहतूत के फल 300px शहतूत (वानस्पतिक नाम: Morus alba) एक फल है। इसका वृक्ष छोटे से लेकर मध्यम आकार का (१० मीटर से २० मीटर ऊँचा) होता है और तेजी से बढ़ता है। इसका जीवनकाल कम होता है। यह चीन का देशज है किन्तु अन्य स्थानों पर भी आसानी से इसकी खेती की जाती है। इसे संस्कृत में 'तूत', मराठी में 'तूती', तुर्की भाषा में 'दूत', तथा फारसी, अजरबैजानी एवं आर्मेनी भाषाओं में 'तूत' कहते हैं रेशम के कीड़ों को खिलाने के लिये सफेद शहतूत की खेती की जाती है। यह भारत के अन्दर खासकर उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश बिहार झारखण्ड मध्य-प्रदेश हरियाणा पंजाब हिमाचल-प्रदेश इत्यादि राज्यों में अत्यधिक इसकी खेती की जाती है। .
देखें फलदार वृक्ष और शहतूत
संतरा (फल)
संतरा एक फल है। संतरे को हाथ से छीलने के बाद पेशीयोँ को अलग कर के चूसकर खाया जा सकता है। सँतरे का रस निकालकर पीया जा सकता है। संतरा ठंडा, तन और मन को प्रसन्नता देने वाला है। उपवास और सभी रोगों में नारंगी दी जा सकती है। जिनकी पाचन शक्ति खराब हो, उनको नारंगी का रस तीन गुने पानी में मिलाकर देना चाहिये। एक व्यक्ति को एक बार में एक या दो नारंगी लेना पर्याप्त है। एक व्यक्ति को जितने विटामिन ‘सी’ की आवश्यकता होती है, वह एक नारंगी प्रतिदिन खाते रहने से पूरी हो जाती है। खांसी-जुकाम होने पर नारंगी के रस का एक गिलास नित्य पीते रहने से लाभ होगा। स्वाद के लिये नमक या मिश्री डालकर पी सकते है। .
देखें फलदार वृक्ष और संतरा (फल)
जामुन
जामुन का पेड़ जामुन (वैज्ञानिक नाम: Syzygium cumini) एक सदाबहार वृक्ष है जिसके फल बैंगनी रंग के होते हैं (लगभग एक से दो सेमी. व्यास के) | यह वृक्ष भारत एवं दक्षिण एशिया के अन्य देशों एवं इण्डोनेशिया आदि में पाया जाता है। इसे विभिन्न घरेलू नामों जैसे जामुन, राजमन, काला जामुन, जमाली, ब्लैकबेरी आदि के नाम से जाना जाता है। प्रकृति में यह अम्लीय और कसैला होता है और स्वाद में मीठा होता है। अम्लीय प्रकृति के कारण सामान्यत: इसे नमक के साथ खाया जता है। जामुन का फल 70 प्रतिशत खाने योग्य होता है। इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मुख्य स्रोत होते हैं। फल में खनिजों की संख्या अधिक होती है। अन्य फलों की तुलना में यह कम कैलोरी प्रदान करता है। एक मध्यम आकार का जामुन 3-4 कैलोरी देता है। इस फल के बीज में काबोहाइट्ररेट, प्रोटीन और कैल्शियम की अधिकता होती है। यह लोहा का बड़ा स्रोत है। प्रति 100 ग्राम में एक से दो मिग्रा आयरन होता है। इसमें विटामिन बी, कैरोटिन, मैग्नीशियम और फाइबर होते हैं। .
देखें फलदार वृक्ष और जामुन
गूलर
गूलर के फल के अन्दर का दृष्य गूलर (Ficus racemosa) फिकस कुल (Ficus) का एक विशाल वृक्ष है। इसे संस्कृत में उडुम्बर, बांग्ला में डुमुर, मराठी में उदुम्बर, गुजराती में उम्बरा, अरबी में जमीझ, फारसी में अंजीरे आदम कहते हैं। इस पर फूल नहीं आते। इसकी शाखाओं में से फल उत्पन्न होते हैं। फल गोल-गोल अंजीर की तरह होते हैं और इसमें से सफेद-सफेद दूध निकलता है। इसके पत्ते लभेड़े के पत्तों जैसे होते हैं। नदी के उदुम्बर के पत्ते और फूल गूलर के पत्तों-फल से छोटे होते हैं। गूलर, २ प्रकार का होता है- नदी उदुम्बर और कठूमर। कठूमर के पत्ते गूलर के पत्तों से बडे होते हैं। इसके पत्तों को छूने से हाथों में खुजली होने लगती है और पत्तों में से दूध निकलता है। .
देखें फलदार वृक्ष और गूलर
आँवला
आँवला, एक स्वास्थ्यवर्धक फल। आंवले की एक डाली पर पत्ते एवं फल साम्राज्य - पादप विभाग - मैंगोलियोफाइटा वर्ग - मैंगोलियोफाइटा जाति - रिबीस प्रजाति - आर यूवा-क्रिस्पा वैज्ञानिक नाम - रिबीस यूवा-क्रिस्पा आँवला एक फल देने वाला वृक्ष है। यह करीब २० फीट से २५ फुट तक लंबा झारीय पौधा होता है। यह एशिया के अलावा यूरोप और अफ्रीका में भी पाया जाता है। हिमालयी क्षेत्र और प्राद्वीपीय भारत में आंवला के पौधे बहुतायत मिलते हैं। इसके फूल घंटे की तरह होते हैं। इसके फल सामान्यरूप से छोटे होते हैं, लेकिन प्रसंस्कृत पौधे में थोड़े बड़े फल लगते हैं। इसके फल हरे, चिकने और गुदेदार होते हैं। स्वाद में इनके फल कसाय होते हैं। संस्कृत में इसे अमृता, अमृतफल, आमलकी, पंचरसा इत्यादि, अंग्रेजी में 'एँब्लिक माइरीबालन' या इण्डियन गूजबेरी (Indian gooseberry) तथा लैटिन में 'फ़िलैंथस एँबेलिका' (Phyllanthus emblica) कहते हैं। यह वृक्ष समस्त भारत में जंगलों तथा बाग-बगीचों में होता है। इसकी ऊँचाई 2000 से 25000 फुट तक, छाल राख के रंग की, पत्ते इमली के पत्तों जैसे, किंतु कुछ बड़े तथा फूल पीले रंग के छोटे-छोटे होते हैं। फूलों के स्थान पर गोल, चमकते हुए, पकने पर लाल रंग के, फल लगते हैं, जो आँवला नाम से ही जाने जाते हैं। वाराणसी का आँवला सब से अच्छा माना जाता है। यह वृक्ष कार्तिक में फलता है। आयुर्वेद के अनुसार हरीतकी (हड़) और आँवला दो सर्वोत्कृष्ट औषधियाँ हैं। इन दोनों में आँवले का महत्व अधिक है। चरक के मत से शारीरिक अवनति को रोकनेवाले अवस्थास्थापक द्रव्यों में आँवला सबसे प्रधान है। प्राचीन ग्रंथकारों ने इसको शिवा (कल्याणकारी), वयस्था (अवस्था को बनाए रखनेवाला) तथा धात्री (माता के समान रक्षा करनेवाला) कहा है। .
देखें फलदार वृक्ष और आँवला
आम
आम एक प्रकार का रसीला फल होता है। इसे भारत में फलों का राजा भी बोलते हैं। इसकी मूल प्रजाति को भारतीय आम कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम मेंगीफेरा इंडिका है। आमों की प्रजाति को मेंगीफेरा कहा जाता है। इस फल की प्रजाति पहले केवल भारतीय उपमहाद्वीप में मिलती थी, इसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों में फैलने लगी। इसका सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है। यह भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल माना जाता है और बांग्लादेश में इसके पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा प्राप्त है। .
देखें फलदार वृक्ष और आम
इमली
इमली, (अंग्रेजी:Tamarind, अरबी: تمر هندي तमर हिन्दी "भारतीय खजूर") पादप कुल फैबेसी का एक वृक्ष है। इसके फल लाल से भूरे रंग के होते हैं, तथा स्वाद में बहुत खट्टे होते हैं। इमली का वृक्ष समय के साथ बहुत बड़ा हो सकता है और इसकी पत्तियाँ एक वृन्त के दोनों तरफ छोटी-छोटी लगी होती हैं। इसके वंश टैमेरिन्डस में सिर्फ एक प्रजाति होती है। .
देखें फलदार वृक्ष और इमली
कटहल
कटहल का पेड़ और उस पर लगे फल कटहल या फनस का वृक्ष शाखायुक्त, सपुष्पक तथा बहुवर्षीय वृक्ष है। यह दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया का मूल-निवासी है। पेड़ पर होने वाले फलों में इसका फल विश्व में सबसे बड़ा होता है। फल के बाहरी सतह पर छोटे-छोटे काँटे पाए जाते हैं। इस प्रकार के संग्रन्थित फल को सोरोसिस कहते हैं। .
देखें फलदार वृक्ष और कटहल
केला
मूसा जाति के घासदार पौधे और उनके द्वारा उत्पादित फल को आम तौर पर केला कहा जाता है। मूल रूप से ये दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णदेशीय क्षेत्र के हैं और संभवतः पपुआ न्यू गिनी में इन्हें सबसे पहले उपजाया गया था। आज, उनकी खेती सम्पूर्ण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। केले के पौधें मुसाके परिवार के हैं। मुख्य रूप से फल के लिए इसकी खेती की जाती है और कुछ हद तक रेशों के उत्पादन और सजावटी पौधे के रूप में भी इसकी खेती की जाती है। चूंकि केले के पौधे काफी लंबे और सामान्य रूप से काफी मजबूत होते हैं और अक्सर गलती से वृक्ष समझ लिए जाते हैं, पर उनका मुख्य या सीधा तना वास्तव में एक छद्मतना होता है। कुछ प्रजातियों में इस छद्मतने की ऊंचाई 2-8 मीटर तक और उसकी पत्तियाँ 3.5 मीटर तक लम्बी हो सकती हैं। प्रत्येक छद्मतना हरे केलों के एक गुच्छे को उत्पन्न कर सकता है, जो अक्सर पकने के बाद पीले या कभी-कभी लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। फल लगने के बाद, छद्मतना मर जाता है और इसकी जगह दूसरा छद्मतना ले लेता है। केले के फल लटकते गुच्छों में ही बड़े होते है, जिनमें 20 फलों तक की एक पंक्ति होती है (जिसे हाथ भी कहा जाता है) और एक गुच्छे में 3-20 केलों की पंक्ति होती है। केलों के लटकते हुए सम्पूर्ण समूह को गुच्छा कहा जाता है, या व्यावसायिक रूप से इसे "बनाना स्टेम" कहा जाता है और इसका वजन 30-50 किलो होता है। एक फल औसतन 125 ग्राम का होता है, जिसमें लगभग 75% पानी और 25% सूखी सामग्री होती है। प्रत्येक फल (केला या 'उंगली' के रूप में ज्ञात) में एक सुरक्षात्मक बाहरी परत होती है (छिलका या त्वचा) जिसके भीतर एक मांसल खाद्य भाग होता है। .
देखें फलदार वृक्ष और केला
अमरूद
लाल अमरूद का फल अमरूद (वानस्पतिक नाम: सीडियम ग्वायवा, प्रजाति सीडियम, जाति ग्वायवा, कुल मिटसी) एक फल देने वाला वृक्ष है। वैज्ञानिकों का विचार है कि अमरूद की उत्पति अमरीका के उष्ण कटिबंधीय भाग तथा वेस्ट इंडीज़ से हुई है। .
देखें फलदार वृक्ष और अमरूद
अंगूर
अंगूर अंगूर (संस्कृत: द्राक्षा) एक फल है। अंगूर एक बलवर्द्धक एवं सौन्दर्यवर्धक फल है। अंगूर फल माँ के दूध के समान पोषक है। फलों में अंगूर सर्वोत्तम माना जाता है। यह निर्बल-सबल, स्वस्थ-अस्वस्थ आदि सभी के लिए समान उपयोगी होता है। ये अंगूर की बेलों पर बड़े-बड़े गुच्छों में उगता है। अंगूर सीधे खाया भी जा सकता है, या फिर उससे अंगूरी शराब भी बनायी जा सकती है, जिसे हाला (अंग्रेज़ी में "वाइन") कहते हैं, यह अंगूर के रस का ख़मीरीकरण करके बनायी जाती है। .
देखें फलदार वृक्ष और अंगूर
उद्यान विज्ञान
फूल ही फूल उद्यान विज्ञान या औद्यानिकी (लैटिन, स्पेनिश, पुर्तगाली:Horticultura, जर्मन:Gartenbau, फ़्रेंच:l'horticulture, अंग्रेजी:Horticulture (हार्टिकल्चर)) में फल, सब्जी, पेड़ तथा फूल, सभी का उगाना सम्मिलित है। इन पादपों के उगाने की कला के अंतर्गत बहुत सी क्रियाएँ आ जाती हैं। .
देखें फलदार वृक्ष और उद्यान विज्ञान
यह भी देखें
खाद्य फल
- अंगूर
- अंजीर
- अनानास
- अनार
- अमरूद
- आम
- कीवी फल
- केला
- तरबूज़
- तेंदू
- फलदार वृक्ष
- फलों की खेती
- फलों की सूची
- बैंगनी मेन्गोस्टीन
- रम्बूटान
- लीची
- शरीफा
फल उत्पादन
- फलदार वृक्ष
वृक्ष
- अर्क
- गुल्म
- चिपको आन्दोलन
- जीवित जड़ सेतु
- ठूंठ
- फलदार वृक्ष
- फलोद्यान
- बोनसाई
- लकड़ी
- वन
- वृक्ष
- वृक्ष रेखा
- वृक्ष विचरण
- वृक्षसंवर्धन
- वृक्षारोपण
- शस्यकर्तन
- सदाबहार