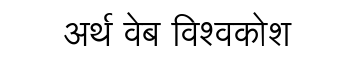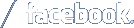14 संबंधों: तद्भव, तुर्की, देशज, देवनागरी, प्राकृत, फ़ारसी भाषा, बज्जिका, मुजफ्फरपुर, शब्दकोश, संस्कृत भाषा, हिन्दी, अरबी, अंग्रेज़ी भाषा, उर्दू भाषा।
तद्भव
तद्भव हिन्दी की एक पत्रिका है। यह पत्रिका हर बार आधुनिक रचनाशीलता पर केन्द्रित एक विशिष्ट संचयन होती है तथा विशुद्ध साहित्यिक सामग्रियों को प्रकाशन में महत्व देती है।.
नई!!: बज्जिका शब्दावली और तद्भव · और देखें »
तुर्की
तुर्की (तुर्क भाषा: Türkiye उच्चारण: तुर्किया) यूरेशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अंकारा है। इसकी मुख्य- और राजभाषा तुर्की भाषा है। ये दुनिया का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो कि धर्मनिर्पेक्ष है। ये एक लोकतान्त्रिक गणराज्य है। इसके एशियाई हिस्से को अनातोलिया और यूरोपीय हिस्से को थ्रेस कहते हैं। स्थिति: 39 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 36 डिग्री पूर्वी देशान्तर। इसका कुछ भाग यूरोप में तथा अधिकांश भाग एशिया में पड़ता है अत: इसे यूरोप एवं एशिया के बीच का 'पुल' कहा जाता है। इजीयन सागर (Aegean sea) के पतले जलखंड के बीच में आ जाने से इस पुल के दो भाग हो जाते हैं, जिन्हें साधारणतया यूरोपीय टर्की तथा एशियाई टर्की कहते हैं। टर्की के ये दोनों भाग बॉसपोरस के जलडमरूमध्य, मारमारा सागर तथा डारडनेल्ज द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। टर्की गणतंत्र का कुल क्षेत्रफल 2,96,185 वर्ग मील है जिसमें यूरोपीय टर्की (पूर्वी थ्रैस) का क्षेत्रफल 9,068 वर्ग मील तथा एशियाई टर्की (ऐनाटोलिआ) का क्षेत्रफल 2,87,117 वर्ग मील है। इसके अंतर्गत 451 दलदली स्थल तथा 3,256 खारे पानी की झीलें हैं। पूर्व में रूस और ईरान, दक्षिण की ओर इराक, सीरिया तथा भूमध्यसागर, पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया और उत्तर में कालासागर इसकी राजनीतिक सीमा निर्धारित करते हैं। यूरोपीय टर्की - त्रिभुजाकर प्रायद्वीपी प्रदेश है जिसका शीर्षक पूर्व में बॉसपोरस के मुहाने पर है। उसके उत्तर तथा दक्षिण दोनों ओर पर्वतश्रेणियाँ फैली हुई हैं। मध्य में निचला मैदान मिलता है जिसमें होकर मारीत्सा और इरजिन नदियाँ बहती हैं। इसी भाग से होकर इस्तैस्म्यूल का संबंध पश्चिमी देशों से है। एशियाई टर्की - इसको हम तीन प्राकृतिक भागों में विभाजित कर सकते हैं: 1.
नई!!: बज्जिका शब्दावली और तुर्की · और देखें »
देशज
हिन्दी या इसकी उपभाषाओं में प्रयुक्त वैसे शब्द, जिनका जन्म स्थानीय तौर पर हुआ है। इनमें क्षेत्रीय बदलाव दिखाई देता है। जैसे- लोटा, थाली, सोंटा, गमछा आदि।.
नई!!: बज्जिका शब्दावली और देशज · और देखें »
देवनागरी
'''देवनागरी''' में लिखी ऋग्वेद की पाण्डुलिपि देवनागरी एक लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएँ तथा कई विदेशी भाषाएं लिखीं जाती हैं। यह बायें से दायें लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है जिसे 'शिरिरेखा' कहते हैं। संस्कृत, पालि, हिन्दी, मराठी, कोंकणी, सिन्धी, कश्मीरी, डोगरी, नेपाली, नेपाल भाषा (तथा अन्य नेपाली उपभाषाएँ), तामाङ भाषा, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली आदि भाषाएँ देवनागरी में लिखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थितियों में गुजराती, पंजाबी, बिष्णुपुरिया मणिपुरी, रोमानी और उर्दू भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। देवनागरी विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त लिपियों में से एक है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की एक ट्राम पर देवनागरी लिपि .
नई!!: बज्जिका शब्दावली और देवनागरी · और देखें »
प्राकृत
सूर्यप्रज्ञप्तिसूत्र । इसकी रचना मूलतः तीसरी-चौथी शताब्दी ईसापूर्व में की गयी थी। भारतीय आर्यभाषा के मध्ययुग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएँ विकसित हुई उनका सामान्य नाम प्राकृत है और उन भाषाओं में जो ग्रंथ रचे गए उन सबको समुच्चय रूप से प्राकृत साहित्य कहा जाता है। विकास की दृष्टि से भाषावैज्ञानिकों ने भारत में आर्यभाषा के तीन स्तर नियत किए हैं - प्राचीन, मध्यकालीन और अर्वाचीन। प्राचीन स्तर की भाषाएँ वैदिक संस्कृत और संस्कृत हैं, जिनके विकास का काल अनुमानत: ई. पू.
नई!!: बज्जिका शब्दावली और प्राकृत · और देखें »
फ़ारसी भाषा
फ़ारसी, एक भाषा है जो ईरान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उज़बेकिस्तान में बोली जाती है। यह ईरान, अफ़ग़ानिस्तान, ताजिकिस्तान की राजभाषा है और इसे ७.५ करोड़ लोग बोलते हैं। भाषाई परिवार के लिहाज़ से यह हिन्द यूरोपीय परिवार की हिन्द ईरानी (इंडो ईरानियन) शाखा की ईरानी उपशाखा का सदस्य है और हिन्दी की तरह इसमें क्रिया वाक्य के अंत में आती है। फ़ारसी संस्कृत से क़ाफ़ी मिलती-जुलती है और उर्दू (और हिन्दी) में इसके कई शब्द प्रयुक्त होते हैं। ये अरबी-फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेज़ों के आगमन से पहले भारतीय उपमहाद्वीप में फ़ारसी भाषा का प्रयोग दरबारी कामों तथा लेखन की भाषा के रूप में होता है। दरबार में प्रयुक्त होने के कारण ही अफ़गानिस्तान में इस दारी कहा जाता है। .
नई!!: बज्जिका शब्दावली और फ़ारसी भाषा · और देखें »
बज्जिका
बज्जिका मैथिली भाषा की उपभाषा है, जो कि बिहार के तिरहुत प्रमंडल में बोली जाती है। इसे अभी तक भाषा का दर्जा नहीं मिला है, मुख्य रूप से यह बोली ही है| भारत में २००१ की जनगणना के अनुसार इन जिलों के लगभग १ करोड़ १५ लाख लोग बज्जिका बोलते हैं। नेपाल के रौतहट एवं सर्लाही जिला एवं उसके आस-पास के तराई क्षेत्रों में बसने वाले लोग भी बज्जिका बोलते हैं। वर्ष २००१ के जनगणना के अनुसार नेपाल में २,३८,००० लोग बज्जिका बोलते हैं। उत्तर बिहार में बोली जाने वाली दो अन्य भाषाएँ भोजपुरी एवं मैथिली के बीच के क्षेत्रों में बज्जिका सेतु रूप में बोली जाती है। .
नई!!: बज्जिका शब्दावली और बज्जिका · और देखें »
मुजफ्फरपुर
मुज़फ्फरपुर उत्तरी बिहार राज्य के तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय तथा मुज़फ्फरपुर ज़िले का प्रमुख शहर एवं मुख्यालय है। अपने सूती वस्त्र उद्योग, लोहे की चूड़ियों, शहद तथा आम और लीची जैसे फलों के उम्दा उत्पादन के लिये यह जिला पूरे विश्व में जाना जाता है, खासकर यहाँ की शाही लीची का कोई जोड़ नहीं है। यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी यहाँ से लीची भेजी जाती है। 2017 मे मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के लिये चयनित हुआ है। अपने उर्वरक भूमि और स्वादिष्ट फलों के स्वाद के लिये मुजफ्फरपुर देश विदेश मे "स्वीटसिटी" के नाम से जाना जाता है। मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट देशभर के सबसे महत्वपूर्ण बिजली उत्पादन केंद्रो मे से एक है। .
नई!!: बज्जिका शब्दावली और मुजफ्फरपुर · और देखें »
शब्दकोश
शब्दकोश (अन्य वर्तनी:शब्दकोष) एक बडी सूची या ऐसा ग्रंथ जिसमें शब्दों की वर्तनी, उनकी व्युत्पत्ति, व्याकरणनिर्देश, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग और पदार्थ आदि का सन्निवेश हो। शब्दकोश एकभाषीय हो सकते हैं, द्विभाषिक हो सकते हैं या बहुभाषिक हो सकते हैं। अधिकतर शब्दकोशों में शब्दों के उच्चारण के लिये भी व्यवस्था होती है, जैसे - अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि में, देवनागरी में या आडियो संचिका के रूप में। कुछ शब्दकोशों में चित्रों का सहारा भी लिया जाता है। अलग-अलग कार्य-क्षेत्रों के लिये अलग-अलग शब्दकोश हो सकते हैं; जैसे - विज्ञान शब्दकोश, चिकित्सा शब्दकोश, विधिक (कानूनी) शब्दकोश, गणित का शब्दकोश आदि। सभ्यता और संस्कृति के उदय से ही मानव जान गया था कि भाव के सही संप्रेषण के लिए सही अभिव्यक्ति आवश्यक है। सही अभिव्यक्ति के लिए सही शब्द का चयन आवश्यक है। सही शब्द के चयन के लिए शब्दों के संकलन आवश्यक हैं। शब्दों और भाषा के मानकीकरण की आवश्यकता समझ कर आरंभिक लिपियों के उदय से बहुत पहले ही आदमी ने शब्दों का लेखाजोखा रखना शुरू कर दिया था। इस के लिए उस ने कोश बनाना शुरू किया। कोश में शब्दों को इकट्ठा किया जाता है। .
नई!!: बज्जिका शब्दावली और शब्दकोश · और देखें »
संस्कृत भाषा
संस्कृत (संस्कृतम्) भारतीय उपमहाद्वीप की एक शास्त्रीय भाषा है। इसे देववाणी अथवा सुरभारती भी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत एक हिंद-आर्य भाषा हैं जो हिंद-यूरोपीय भाषा परिवार का एक शाखा हैं। आधुनिक भारतीय भाषाएँ जैसे, हिंदी, मराठी, सिन्धी, पंजाबी, नेपाली, आदि इसी से उत्पन्न हुई हैं। इन सभी भाषाओं में यूरोपीय बंजारों की रोमानी भाषा भी शामिल है। संस्कृत में वैदिक धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्मग्रंथ लिखे गये हैं। बौद्ध धर्म (विशेषकर महायान) तथा जैन मत के भी कई महत्त्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में लिखे गये हैं। आज भी हिंदू धर्म के अधिकतर यज्ञ और पूजा संस्कृत में ही होती हैं। .
नई!!: बज्जिका शब्दावली और संस्कृत भाषा · और देखें »
हिन्दी
हिन्दी या भारतीय विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राजभाषा है। केंद्रीय स्तर पर दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। यह हिन्दुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप है जिसमें संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्द का प्रयोग अधिक हैं और अरबी-फ़ारसी शब्द कम हैं। हिन्दी संवैधानिक रूप से भारत की प्रथम राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। हालांकि, हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है क्योंकि भारत का संविधान में कोई भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया था। चीनी के बाद यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार यह विश्व की दस शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। हिन्दी और इसकी बोलियाँ सम्पूर्ण भारत के विविध राज्यों में बोली जाती हैं। भारत और अन्य देशों में भी लोग हिन्दी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। फ़िजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम की और नेपाल की जनता भी हिन्दी बोलती है।http://www.ethnologue.com/language/hin 2001 की भारतीय जनगणना में भारत में ४२ करोड़ २० लाख लोगों ने हिन्दी को अपनी मूल भाषा बताया। भारत के बाहर, हिन्दी बोलने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका में 648,983; मॉरीशस में ६,८५,१७०; दक्षिण अफ्रीका में ८,९०,२९२; यमन में २,३२,७६०; युगांडा में १,४७,०००; सिंगापुर में ५,०००; नेपाल में ८ लाख; जर्मनी में ३०,००० हैं। न्यूजीलैंड में हिन्दी चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों में १४ करोड़ १० लाख लोगों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू, मौखिक रूप से हिन्दी के काफी सामान है। लोगों का एक विशाल बहुमत हिन्दी और उर्दू दोनों को ही समझता है। भारत में हिन्दी, विभिन्न भारतीय राज्यों की १४ आधिकारिक भाषाओं और क्षेत्र की बोलियों का उपयोग करने वाले लगभग १ अरब लोगों में से अधिकांश की दूसरी भाषा है। हिंदी हिंदी बेल्ट का लिंगुआ फ़्रैंका है, और कुछ हद तक पूरे भारत (आमतौर पर एक सरल या पिज्जाइज्ड किस्म जैसे बाजार हिंदुस्तान या हाफ्लोंग हिंदी में)। भाषा विकास क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी हिन्दी प्रेमियों के लिए बड़ी सन्तोषजनक है कि आने वाले समय में विश्वस्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की जो चन्द भाषाएँ होंगी उनमें हिन्दी भी प्रमुख होगी। 'देशी', 'भाखा' (भाषा), 'देशना वचन' (विद्यापति), 'हिन्दवी', 'दक्खिनी', 'रेखता', 'आर्यभाषा' (स्वामी दयानन्द सरस्वती), 'हिन्दुस्तानी', 'खड़ी बोली', 'भारती' आदि हिन्दी के अन्य नाम हैं जो विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डों में एवं विभिन्न सन्दर्भों में प्रयुक्त हुए हैं। .
नई!!: बज्जिका शब्दावली और हिन्दी · और देखें »
अरबी
अरबी बहुविकल्पी शब्द है जिस्का संबंध निम्नलिखित पृष्ठों से होता है। साहित्य और धर्म में-.
नई!!: बज्जिका शब्दावली और अरबी · और देखें »
अंग्रेज़ी भाषा
अंग्रेज़ी भाषा (अंग्रेज़ी: English हिन्दी उच्चारण: इंग्लिश) हिन्द-यूरोपीय भाषा-परिवार में आती है और इस दृष्टि से हिंदी, उर्दू, फ़ारसी आदि के साथ इसका दूर का संबंध बनता है। ये इस परिवार की जर्मनिक शाखा में रखी जाती है। इसे दुनिया की सर्वप्रथम अन्तरराष्ट्रीय भाषा माना जाता है। ये दुनिया के कई देशों की मुख्य राजभाषा है और आज के दौर में कई देशों में (मुख्यतः भूतपूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों में) विज्ञान, कम्प्यूटर, साहित्य, राजनीति और उच्च शिक्षा की भी मुख्य भाषा है। अंग्रेज़ी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। यह एक पश्चिम जर्मेनिक भाषा है जिसकी उत्पत्ति एंग्लो-सेक्सन इंग्लैंड में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के 19 वीं शताब्दी के पूर्वार्ध और ब्रिटिश साम्राज्य के 18 वीं, 19 वीं और 20 वीं शताब्दी के सैन्य, वैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव के परिणाम स्वरूप यह दुनिया के कई भागों में सामान्य (बोलचाल की) भाषा बन गई है। कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों और राष्ट्रमंडल देशों में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल एक द्वितीय भाषा और अधिकारिक भाषा के रूप में होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से, अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति ५वीं शताब्दी की शुरुआत से इंग्लैंड में बसने वाले एंग्लो-सेक्सन लोगों द्वारा लायी गयी अनेक बोलियों, जिन्हें अब पुरानी अंग्रेजी कहा जाता है, से हुई है। वाइकिंग हमलावरों की प्राचीन नोर्स भाषा का अंग्रेजी भाषा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। नॉर्मन विजय के बाद पुरानी अंग्रेजी का विकास मध्य अंग्रेजी के रूप में हुआ, इसके लिए नॉर्मन शब्दावली और वर्तनी के नियमों का भारी मात्र में उपयोग हुआ। वहां से आधुनिक अंग्रेजी का विकास हुआ और अभी भी इसमें अनेक भाषाओँ से विदेशी शब्दों को अपनाने और साथ ही साथ नए शब्दों को गढ़ने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। एक बड़ी मात्र में अंग्रेजी के शब्दों, खासकर तकनीकी शब्दों, का गठन प्राचीन ग्रीक और लैटिन की जड़ों पर आधारित है। .
नई!!: बज्जिका शब्दावली और अंग्रेज़ी भाषा · और देखें »
उर्दू भाषा
उर्दू भाषा हिन्द आर्य भाषा है। उर्दू भाषा हिन्दुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप मानी जाती है। उर्दू में संस्कृत के तत्सम शब्द न्यून हैं और अरबी-फ़ारसी और संस्कृत से तद्भव शब्द अधिक हैं। ये मुख्यतः दक्षिण एशिया में बोली जाती है। यह भारत की शासकीय भाषाओं में से एक है, तथा पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है। इस के अतिरिक्त भारत के राज्य तेलंगाना, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त शासकीय भाषा है। .
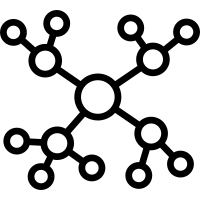
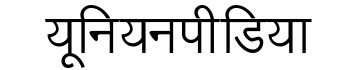

 ब्राउज़र की तुलना में तेजी से पहुँच!
ब्राउज़र की तुलना में तेजी से पहुँच!