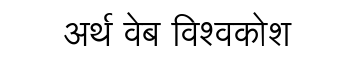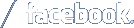19 संबंधों: तुहफ़तुल हिन्द, दामोदर पंडित, नागरीप्रचारिणी सभा, प्रभाकर माचवे, महाभाष्य, योन योस्वा केटलार, रूसी भाषा, संस्कृत व्याकरण का इतिहास, हिन्दी, हिन्दी व्याकरण, व्याकरण, ग्रामाटिका हिन्दोस्तानिका, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र वर्मा, कामताप्रसाद गुरु, काशी, किशोरीदास वाजपेयी, अष्टाध्यायी, उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण।
तुहफ़तुल हिन्द
तुहफ़तुल हिन्द मिर्ज़ा ख़ान का ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। हिन्दी व्याकरण के इतिहास में इस ग्रंथ को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मिर्ज़ा ख़ान ने ब्रज भाषा का एक व्याकरण १६७५ ई. से कुछ पूर्व रचा था। यह व्याकरण बहुत ही संक्षिप्त (केवल 16 पृष्ठों का) है और फारसी भाषा में लिखी उसकी मूल रचना "तुहफ़तुल-हिन्द" (हिन्दुस्तान का तोहफ़ा) का एक अंश है। तुहफ़तुल-हिन्द में तत्कालीन हिन्दी साहित्य के विविध विषयों का विवेचन है जो क्रमशः इस प्रकार हैं - व्याकरण, छन्द, तुक, अलंकार, शृंगार रस, संगीत, कामशास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र और शब्दकोष। हिन्दी-फारसी शब्दकोश में तीन हजार से कुछ अधिक शब्द हैं। मीर्ज़ा ख़ान ने इस बात का बहुत खयाल रखा है कि दिये गये हिन्दी शब्दों की वर्तनी में कोई गलती न हो। इसके लिए उसने अपनी रचना के प्रत्येक शब्द की वर्तनी अपने विशिष्ट लिप्यंतरण के रूप में दी है। उदाहरणस्वरूप - फारसी/अरबी के 'वाव्' अक्षर का प्रयोग 'ऊ' (जैसे 'नूर' में) और 'ओ' (जैसे 'शोर' में) दोनों ध्वनियों के लिए किया जाता है। प्रथम ध्वनि के लिए वह 'वाव्-ए-मरूफ़' और दूसरे के लिए 'वाव्-ए-मज्हूल' शब्द का प्रयोग करता है। पूर्ण अनुनासिक ध्वनि (जैसे 'माँ' 'भँवरा' में) एवं अपूर्ण अनुनासिक ध्वनि (जैसे 'गंगा' में) - इन दोनों के लिए फारसी/अरबी लिपि में सिर्फ 'नून' अक्षर है। मीर्ज़ा ख़ान ने इन दोनों ध्वनियों के लिए 'नून' में अलग-अलग विशिष्ट चिह्न देकर अन्तर दर्शाया है। मीर्ज़ा ख़ान का विभिन्न विषयों का विवेचन संतोषजनक रूप से वैज्ञानिक एवं विस्तृत है। भाषाशास्त्र के विचार से उसका कोश देशी भाषाओं के विश्लेषण में रुचि रखनेवालों के लिए बहुत उपयोगी है। अपनी भूमिका में मीर्ज़ा ख़ान ने हिन्दी वर्णमाला का विस्तृत विवेचन किया है। यथोचित व्याकरण अंग्रेजी अनुवाद भाग में कुल 16 पृष्ठों (पृ. 53-91) का है। इस व्याकरण का फारसी शीर्षक (पृ. 51) है - "क़वाइदे कुल्लियः भाखा" (अर्थात् 'भाखा के व्याकरणिक नियम')। क़वाइद का विवेचन भूमिका के चौथे अध्याय के दूसरे भाग में है, जिसमें कुल दश अनुच्छेद हैं। पहले अनुच्छेद में ब्रज भाषा की स्थिति का वर्णन है। लेखक सभी भाषाओं में इस भाषा की विशेष प्रशंसा करता है, क्योंकि यह कवियों और संस्कृत लोगों की भाषा है। इसी कारण लेखक इस भाषा के व्याकरणिक नियमों की रचना करने का निश्चय करता है। दूसरे अनुच्छेद में शब्द और उसके प्रकार का विवेचन है। तीसरे और चौथे अनुच्छेदों में प्रत्ययों सहित क्रमशः पुलिंग (.
नई!!: हिन्दी व्याकरण का इतिहास और तुहफ़तुल हिन्द · और देखें »
दामोदर पंडित
दामोदर पण्डित हिन्दी के प्रथम वैयाकरण थे। उनके द्वारा रचित उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण हिंदी-व्याकरण का पहला ग्रंथ है। इसका रचना काल १२वीं शती का पूर्वार्द्ध माना जाता है। दामोदर पण्डित बनारस के निवासी थे। श्रेणी:हिन्दी श्रेणी:वैयाकरण.
नई!!: हिन्दी व्याकरण का इतिहास और दामोदर पंडित · और देखें »
नागरीप्रचारिणी सभा
नागरीप्रचारिणी सभा, हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति तथा प्रचार और प्रसार करनेवाली भारत की अग्रणी संस्था है। भारतेन्दु युग के अनंतर हिंदी साहित्य की जो उल्लेखनीय प्रवृत्तियाँ रही हैं उन सबके नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण योग रहा है। .
नई!!: हिन्दी व्याकरण का इतिहास और नागरीप्रचारिणी सभा · और देखें »
प्रभाकर माचवे
डॉ प्रभाकर माचवे (1917 - 1991) हिन्दी के साहित्यकार थे। उनका जन्म ग्वालियर में हुआ एवं शिक्षा इंदौर में हुई। .
नई!!: हिन्दी व्याकरण का इतिहास और प्रभाकर माचवे · और देखें »
महाभाष्य
पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखी जिसे व्याकरणमहाभाष्य का नाम दिया (महा+भाष्य (समीक्षा, टिप्पणी, विवेचना, आलोचना))। व्याकरण महाभाष्य में कात्यायन वार्तिक भी सम्मिलित हैं जो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर कात्यायन के भाष्य हैं। कात्यायन के वार्तिक कुल लगभग १५०० हैं जो अन्यत्र नहीं मिलते बल्कि केवल व्याकरणमहाभाष्य में पतंजलि द्वारा सन्दर्भ के रूप में ही उपलब्ध हैं। संस्कृत के तीन महान वैयाकरणों में पतंजलि भी हैं। अन्य दो हैं - पाणिनि तथा कात्यायन (१५० ईशा पूर्व)। महाभाष्य में शिक्षा (phonology, including accent), व्याकरण (grammar and morphology) और निरुक्त (etymology) - तीनों की चर्चा हुई है। .
नई!!: हिन्दी व्याकरण का इतिहास और महाभाष्य · और देखें »
योन योस्वा केटलार
जान जेशुआ केटलेर (1659-1718) या योन योस्वा केटलार (En:Joan Josua Ketelaar), का नाम डच भाषा में लिखे गए उनके हिंदी व्याकरण के ग्रंथ के लिए जाना जाता है। योन योस्वा केटलार का पारिवारिक नाम केटलर था, उसका जन्म पूर्वी प्रशिया (आधुनिक पोलैंड) के एल्बिंग नामक नगर में 1659 ई. में हुआ था और उसकी मृत्यु 1718 में फारस (ईरान) में। वह सन् 1683 में भारत आया था और डच इस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्लर्क, असिस्टेंट (1687), अकाउंटेंट (1696), बुक कीपर (1699), प्रोविज़नल 'चीफ़' (1700), जुनियर मर्चेंट (1701), मर्चेंट (1706), सीनियर मर्चेंट (1708), दूत (1708), डिरेक्टर ऑव् ट्रेड (1711), राजदूत (1716) पदों पर कार्य किया। इस दौरान उसे सूरत, भरुच, अहमदाबाद, आगरा एवं लखनऊ में रहने का अवसर मिला। आगरा निवास के समय उसने हिन्दी व्याकरण डच भाषा में लिखा, जिसकी प्रतिलिपि उसके सहायक इजाक फान देअर हीव ने 1698 ई. में लखनऊ में प्रकाशित की। सन् 1743 में इसका लैटिन अनुवाद डैविड मिल ने प्रकाशित करवाया। इसी लैटिन अनुवाद से पहली बार यह व्याकरण प्रकाश में आया। डॉ॰ सुनीति कुमार चटर्जी ने इस लैटिन अनुवाद का अनुशीलन कर अपना लेख "The Oldest Grammar of Hindustani" प्रकाशित करवाया। लइदन (Leyden) विश्वविद्यालय के डॉ॰ फ़ॉग़ल ने मूल डच भाषा में लिखित हिन्दी व्याकरण का अनुशीलन कर अपने दो लेख "The Author of the First Grammar of Hindustani" और "Joan Josua Ketelaar of Elbing, Author of the First Hindustani Grammar"14 प्रकाशित कराये। केटलार की जीवनी और उसके हिन्दी व्याकरण की विस्तृत चर्चा प्रकृत लेखक के "हिन्दी भाषा का प्रथम व्याकरण" नामक लेख में की गयी है। .
नई!!: हिन्दी व्याकरण का इतिहास और योन योस्वा केटलार · और देखें »
रूसी भाषा
विश्व में रूसी भाषा का प्रसार रूसी भाषा (русский язык,रूस्किय् यज़ीक्) - पूर्वी स्लाविक भाषाओं में सर्वाधिक प्रचलित भाषा है। रूसी यूरोप की एक प्रमुख भाषा तो है ही, विश्व की प्रमुख भाषाओं में भी इस का विशेष स्थान है, हालाँकि भौगोलिक दृष्टि से रूसी बोलने वालों की अधिकतर संख्या यूरोप की बजाय एशिया में निवास करती है। रूसी भाषा रूसी संघ की आधिकारिक भाषा है। इसके अतिरिक्त बेलारूस, कज़ाकिस्तान, क़िर्गिस्तान, उक्राइनी स्वायत्त जनतंत्र क्रीमिया, जॉर्जियाई अस्वीकृत जनतंत्र अब्ख़ाज़िया और दक्षिणी ओसेतिया, मल्दावियाई अस्वीकृत जनतंत्र ट्रांसनीस्ट्रिया (नीस्टर का क्षेत्र) और स्वायत्त जनतंत्र गगऊज़िया नामक देशों और जनतंत्रों में रूसी भाषा सहायक आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार की गई है। रूसी भूतपूर्व सोवियत संघ के सभी १५ सोवियत समाजवादी जनतंत्रों की राजकीय भाषा थी। सन् 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद भी इन सभी आधुनिक स्वतंत्र देशों में अपनी-अपनी राष्ट्रीय भाषाओं के साथ-साथ परस्पर आपसी व्यवहार के लिए सम्पर्क भाषा के रूप में रूसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इन १५ देशों में रहने वाले निवासियों में से भी अधिकांश की मातृभाषा रूसी ही है। विश्व के विभिन्न देशों में (इसराइल, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि) जहाँ कहीं भी भूतपूर्व सोवियत संघ या रूस के प्रवासी बसे हुए हैं, वहाँ कई जगहों पर रूसी पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं, रूसी भाषा में रेडियो और दूरदर्शन काम करते हैं तथा स्कूलों में रूसी सिखाई जाती है। कुछ वर्ष पहले तक पूर्वी यूरोपियाई देशों के स्कूलों में रूसी भाषा विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती थी। कुल मिला कर विश्व में रूसी भाषा बोलने वालों की संख्या ३०-३५ करोड़ है, जिस में से 16 करोड़ लोग इसे अपनी मातृभाषा मानते हैं। इसके आधार पर रूसी संसार की भाषाओं में पाँचवे स्थान पर है और वह संयुक्त राष्ट्र (UN) की ५ आधिकारिक भाषाओं में से एक है। .
नई!!: हिन्दी व्याकरण का इतिहास और रूसी भाषा · और देखें »
संस्कृत व्याकरण का इतिहास
संस्कृत का व्याकरण वैदिक काल में ही स्वतंत्र विषय बन चुका था। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात - ये चार आधारभूत तथ्य यास्क (ई. पू. लगभग 700) के पूर्व ही व्याकरण में स्थान पा चुके थे। पाणिनि (ई. पू. लगभग 550) के पहले कई व्याकरण लिखे जा चुके थे जिनमें केवल आपिशलि और काशकृत्स्न के कुछ सूत्र आज उपलब्ध हैं। किंतु संस्कृत व्याकरण का क्रमबद्ध इतिहास पाणिनि से आरंभ होता है। व्याकरण शास्त्र का वृहद् इतिहास है किन्तु महामुनि पाणिनि और उनके द्वारा प्रणीत अष्टाधयायी ही इसका केन्द्र बिन्दु हैं। पाणिनि ने अष्टाधयायी में 3995 सूत्रें की रचनाकर भाषा के नियमों को व्यवस्थित किया जिसमें वाक्यों में पदों का संकलन, पदों का प्रकृति, प्रत्यय विभाग एवं पदों की रचना आदि प्रमुख तत्त्व हैं। इन नियमों की पूर्त्ति के लिये धातु पाठ, गण पाठ तथा उणादि सूत्र भी पाणिनि ने बनाये। सूत्रों में उक्त, अनुक्त एवं दुरुक्त विषयों का विचार कर कात्यायन ने वार्त्तिक की रचना की। बाद में महामुनि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना कर संस्कृत व्याकरण को पूर्णता प्रदान की। इन्हीं तीनों आचार्यों को 'त्रिमुनि' के नाम से जाना जाता है। प्राचीन व्याकरण में इनका अनिवार्यतः अधययन किया जाता है। नव्य व्याकरण के अन्तर्गत प्रक्रिया क्रम के अनुसार शास्त्रों का अधययन किया जाता है जिसमें भट्टोजीदीक्षित, नागेश भट्ट आदि आचार्यों के ग्रन्थों का अधययन मुख्य है। प्राचीन व्याकरण एवं नव्य व्याकरण दो स्वतंत्र विषय हैं। .
नई!!: हिन्दी व्याकरण का इतिहास और संस्कृत व्याकरण का इतिहास · और देखें »
हिन्दी
हिन्दी या भारतीय विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राजभाषा है। केंद्रीय स्तर पर दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। यह हिन्दुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप है जिसमें संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्द का प्रयोग अधिक हैं और अरबी-फ़ारसी शब्द कम हैं। हिन्दी संवैधानिक रूप से भारत की प्रथम राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। हालांकि, हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है क्योंकि भारत का संविधान में कोई भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया था। चीनी के बाद यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार यह विश्व की दस शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। हिन्दी और इसकी बोलियाँ सम्पूर्ण भारत के विविध राज्यों में बोली जाती हैं। भारत और अन्य देशों में भी लोग हिन्दी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। फ़िजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम की और नेपाल की जनता भी हिन्दी बोलती है।http://www.ethnologue.com/language/hin 2001 की भारतीय जनगणना में भारत में ४२ करोड़ २० लाख लोगों ने हिन्दी को अपनी मूल भाषा बताया। भारत के बाहर, हिन्दी बोलने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका में 648,983; मॉरीशस में ६,८५,१७०; दक्षिण अफ्रीका में ८,९०,२९२; यमन में २,३२,७६०; युगांडा में १,४७,०००; सिंगापुर में ५,०००; नेपाल में ८ लाख; जर्मनी में ३०,००० हैं। न्यूजीलैंड में हिन्दी चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों में १४ करोड़ १० लाख लोगों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू, मौखिक रूप से हिन्दी के काफी सामान है। लोगों का एक विशाल बहुमत हिन्दी और उर्दू दोनों को ही समझता है। भारत में हिन्दी, विभिन्न भारतीय राज्यों की १४ आधिकारिक भाषाओं और क्षेत्र की बोलियों का उपयोग करने वाले लगभग १ अरब लोगों में से अधिकांश की दूसरी भाषा है। हिंदी हिंदी बेल्ट का लिंगुआ फ़्रैंका है, और कुछ हद तक पूरे भारत (आमतौर पर एक सरल या पिज्जाइज्ड किस्म जैसे बाजार हिंदुस्तान या हाफ्लोंग हिंदी में)। भाषा विकास क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी हिन्दी प्रेमियों के लिए बड़ी सन्तोषजनक है कि आने वाले समय में विश्वस्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की जो चन्द भाषाएँ होंगी उनमें हिन्दी भी प्रमुख होगी। 'देशी', 'भाखा' (भाषा), 'देशना वचन' (विद्यापति), 'हिन्दवी', 'दक्खिनी', 'रेखता', 'आर्यभाषा' (स्वामी दयानन्द सरस्वती), 'हिन्दुस्तानी', 'खड़ी बोली', 'भारती' आदि हिन्दी के अन्य नाम हैं जो विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डों में एवं विभिन्न सन्दर्भों में प्रयुक्त हुए हैं। .
नई!!: हिन्दी व्याकरण का इतिहास और हिन्दी · और देखें »
हिन्दी व्याकरण
हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध करानेवाला शास्त्र है। यह हिंदी भाषा के अध्ययन का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें हिंदी के सभी स्वरूपों का चार खंडों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है; यथा- वर्ण विचार के अंतर्गत ध्वनि और वर्ण तथा शब्द विचार के अंतर्गत शब्द के विविध पक्षों संबंधी नियमों और वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य संबंधी विभिन्न स्थितियों एवं छंद विचार में साहित्यिक रचनाओं के शिल्पगत पक्षों पर विचार किया गया है। .
नई!!: हिन्दी व्याकरण का इतिहास और हिन्दी व्याकरण · और देखें »
व्याकरण
किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन व्याकरण (ग्रामर) कहलाता है। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना आता है। किसी भी भाषा के लिखने, पढ़ने और बोलने के निश्चित नियम होते हैं। भाषा की शुद्धता व सुंदरता को बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। ये नियम भी व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। व्याकरण भाषा के अध्ययन का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। किसी भी "भाषा" के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन "व्याकरण" कहलाता है, जैसे कि शरीर के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन "शरीरशास्त्र" और किसी देश प्रदेश आदि का वर्णन "भूगोल"। यानी व्याकरण किसी भाषा को अपने आदेश से नहीं चलाता घुमाता, प्रत्युत भाषा की स्थिति प्रवृत्ति प्रकट करता है। "चलता है" एक क्रियापद है और व्याकरण पढ़े बिना भी सब लोग इसे इसी तरह बोलते हैं; इसका सही अर्थ समझ लेते हैं। व्याकरण इस पद का विश्लेषण करके बताएगा कि इसमें दो अवयव हैं - "चलता" और "है"। फिर वह इन दो अवयवों का भी विश्लेषण करके बताएगा कि (च् अ ल् अ त् आ) "चलता" और (ह अ इ उ) "है" के भी अपने अवयव हैं। "चल" में दो वर्ण स्पष्ट हैं; परंतु व्याकरण स्पष्ट करेगा कि "च" में दो अक्षर है "च्" और "अ"। इसी तरह "ल" में भी "ल्" और "अ"। अब इन अक्षरों के टुकड़े नहीं हो सकते; "अक्षर" हैं ये। व्याकरण इन अक्षरों की भी श्रेणी बनाएगा, "व्यंजन" और "स्वर"। "च्" और "ल्" व्यंजन हैं और "अ" स्वर। चि, ची और लि, ली में स्वर हैं "इ" और "ई", व्यंजन "च्" और "ल्"। इस प्रकार का विश्लेषण बड़े काम की चीज है; व्यर्थ का गोरखधंधा नहीं है। यह विश्लेषण ही "व्याकरण" है। व्याकरण का दूसरा नाम "शब्दानुशासन" भी है। वह शब्दसंबंधी अनुशासन करता है - बतलाता है कि किसी शब्द का किस तरह प्रयोग करना चाहिए। भाषा में शब्दों की प्रवृत्ति अपनी ही रहती है; व्याकरण के कहने से भाषा में शब्द नहीं चलते। परंतु भाषा की प्रवृत्ति के अनुसार व्याकरण शब्दप्रयोग का निर्देश करता है। यह भाषा पर शासन नहीं करता, उसकी स्थितिप्रवृत्ति के अनुसार लोकशिक्षण करता है। .
नई!!: हिन्दी व्याकरण का इतिहास और व्याकरण · और देखें »
ग्रामाटिका हिन्दोस्तानिका
ग्रामाटिका हिन्दोस्तानिका हिन्दी व्याकरण की पुस्तक है जिसे डेनमार्क से भारत आये ईसाई मिशनरी डॉ॰ बेंजामिन शूल्ज़ ने तैयार किया था। डेनिश भाषी डॉ॰ शूल्ज़ प्रोटेस्टेन्ट मिशनरी थे। ये पहले तमिलनाडु में कार्यरत थे, बाद में हैदराबाद आ गए। आपकी मृत्यु सन् 1760 ई0 में जर्मनी के हाले नगर में हुई। कार्य करते हुए इनको दायित्व-बोध हुआ कि भारत में आने वाले मिशनरियों को हिन्दुस्तानी भाषा से अवगत कराना चाहिए। हिन्दुस्तानी भाषा के सम्बन्ध में लेखक ने अपनी भूमिका में लिखा, ‘‘यह भाषा अपने आप में बहुत ही सरल है। मैं जब यह भाषा सीखने लगा तो मुझे अत्यधिक कठिनाई का अनुभव हुआ.............
नई!!: हिन्दी व्याकरण का इतिहास और ग्रामाटिका हिन्दोस्तानिका · और देखें »
गौरीशंकर हीराचंद ओझा
डॉ गौरीशंकर हीराचंद ओझा डॉ गौरीशंकर हीराचंद ओझा (1863-1947) भारत के इतिहासकार एवं हिन्दी लेखक थे। डॉ॰ ओझा राजस्थान क्षेत्र के मार्गशोधक इतिहास लेखकों में गिने जाते हैं। आपका जन्म सिरोही के रोहिड़ा ग्राम में हुआ था। आपने राजस्थान तथा भारत के इतिहास सम्बन्धी अनेक पुस्तकें लिखी थी। कविराज श्यामलदास ने आपको उदयपुर के इतिहास विभाग में नियुक्त किया था। ओझाजी कविराज श्यामलदास को अपना गुरु मानते थे। 17 अप्रैल, 1947 ई० को अपनी जन्मभूमि रोहिड़ा में ही ओझा जी का देहावसान हो गया। .
नई!!: हिन्दी व्याकरण का इतिहास और गौरीशंकर हीराचंद ओझा · और देखें »
आचार्य रामचंद्र वर्मा
आचार्य रामचंद्र वर्मा (1890-1969 ई.) हिन्दी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे हैं। हिन्दी शब्दसागर के सम्पादकमण्डल के प्रमुख सदस्य थे। आपने आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के साथ मिलकर 'अच्छी हिन्दी' का आन्दोलन चलाया। आपके समय में हिन्दी का मानकीकरण हुआ। .
नई!!: हिन्दी व्याकरण का इतिहास और आचार्य रामचंद्र वर्मा · और देखें »
कामताप्रसाद गुरु
कामताप्रसाद गुरु (१८७५ - १९४७ ई.) हिंदी के लब्धप्रतिष्ठ वैयाकरण तथा साहित्यकार। .
नई!!: हिन्दी व्याकरण का इतिहास और कामताप्रसाद गुरु · और देखें »
काशी
काशी जैनों का मुख्य तीर्थ है यहाँ श्री पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ एवम श्री समन्तभद्र स्वामी ने अतिशय दिखाया जैसे ही लोगों ने नमस्कार करने को कहा पिंडी फट गई और उसमे से श्री चंद्रप्रभु की प्रतिमा जी निकली जो पिन्डि आज भी फटे शंकर के नाम से प्रसिद्ध है काशी विश्वनाथ मंदिर (१९१५) काशी नगरी वर्तमान वाराणसी शहर में स्थित पौराणिक नगरी है। इसे संसार के सबसे पुरानी नगरों में माना जाता है। भारत की यह जगत्प्रसिद्ध प्राचीन नगरी गंगा के वाम (उत्तर) तट पर उत्तर प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी कोने में वरुणा और असी नदियों के गंगासंगमों के बीच बसी हुई है। इस स्थान पर गंगा ने प्राय: चार मील का दक्षिण से उत्तर की ओर घुमाव लिया है और इसी घुमाव के ऊपर इस नगरी की स्थिति है। इस नगर का प्राचीन 'वाराणसी' नाम लोकोच्चारण से 'बनारस' हो गया था जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शासकीय रूप से पूर्ववत् 'वाराणसी' कर दिया है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है - 'काशिरित्ते..
नई!!: हिन्दी व्याकरण का इतिहास और काशी · और देखें »
किशोरीदास वाजपेयी
आचार्य किशोरीदास वाजपेयी आचार्य किशोरीदास वाजपेयी (१८९८-१९८१) हिन्दी के साहित्यकार एवं सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। हिन्दी की खड़ी बोली के व्याकरण की निर्मिति में पूर्ववर्ती भाषाओं के व्याकरणाचार्यो द्वारा निर्धारित नियमों और मान्यताओं का उदारतापूर्वक उपयोग करके इसके मानक स्वरूप को वैज्ञानिक दृष्टि से सम्पन्न करने का गुरुतर दायित्व पं॰ किशोरीदास वाजपेयी ने निभाया। इसीलिए उन्हें 'हिन्दी का पाणिनी' कहा जाता है। अपनी तेजस्विता व प्रतिभा से उन्होंने साहित्यजगत को आलोकित किया और एक महान भाषा के रूपाकार को निर्धारित किया। आचार्य किशोरीदास बाजपेयी ने हिन्दी को परिष्कृत रूप प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनसे पूर्व खडी बोली हिन्दी का प्रचलन तो हो चुका था पर उसका कोई व्यवस्थित व्याकरण नहीं था। अत: आपने अपने अथक प्रयास एवं ईमानदारी से भाषा का परिष्कार करते हुए व्याकरण का एक सुव्यवस्थित रूप निर्धारित कर भाषा का परिष्कार तो किया ही साथ ही नये मानदण्ड भी स्थापित किये। स्वाभाविक है भाषा को एक नया स्वरूप मिला। अत: हिन्दी क्षेत्र में आपको "पाणिनि' संज्ञा से अभिहित किया जाने लगा। .
नई!!: हिन्दी व्याकरण का इतिहास और किशोरीदास वाजपेयी · और देखें »
अष्टाध्यायी
अष्टाध्यायी (अष्टाध्यायी .
नई!!: हिन्दी व्याकरण का इतिहास और अष्टाध्यायी · और देखें »
उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण
उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण दामोदर पंडित द्वारा रचित हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है। हिन्दी व्याकरण के इतिहास में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसका रचना काल १२वीं शती का पूर्वार्द्ध माना जाता है। प्राचीनतम हिन्दी-व्याकरण सत्रहवीं शताब्दी का है, जबकि साहित्य का आदिकाल लगभग दशवीं-ग्यारहवीं शताब्दी से माना जाता है। ऐसी स्थिति में हिन्दी भाषा के क्रमिक विकास एवं इतिहास के विचार से बारहवीं शती के प्रारम्भ में बनारस के दामोदर पंडित द्वारा रचित द्विभाषिक ग्रंथ 'उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण'6 का विशेष महत्त्व है। यह ग्रंथ हिन्दी की पुरानी कोशली या अवधी बोली बोलने वालों के लिए संस्कृत सिखाने वाला एक मैनुअल है, जिसमें पुरानी अवधी के व्याकरणिक रूपों के समानान्तर संस्कृत रूपों के साथ पुरानी कोशली एवं संस्कृत दोनों में उदाहरणात्मक वाक्य दिये गये हैं। उदाहरणस्वरूपः-.
नई!!: हिन्दी व्याकरण का इतिहास और उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण · और देखें »
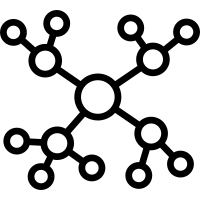
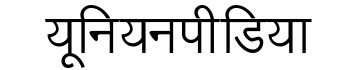

 ब्राउज़र की तुलना में तेजी से पहुँच!
ब्राउज़र की तुलना में तेजी से पहुँच!