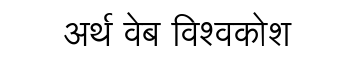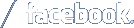10 संबंधों: चन्द्रमा, तमिल नाडु, दृग्गणित, परहितकरण, पंचांग, संस्कृत भाषा, संगमग्राम के माधव, वररुचि, वेण्वारोह, कटपयादि संख्या।
चन्द्रमा
कोई विवरण नहीं।
नई!!: चन्द्रवाक्य और चन्द्रमा · और देखें »
तमिल नाडु
तमिल नाडु (तमिल:, तमिऴ् नाडु) भारत का एक दक्षिणी राज्य है। तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई (चेऩ्ऩै) है। तमिल नाडु के अन्य महत्त्वपूर्ण नगर मदुरै, त्रिचि (तिरुच्चि), कोयम्बतूर (कोऽयम्बुत्तूर), सेलम (सेऽलम), तिरूनेलवेली (तिरुनेल्वेऽली) हैं। इसके पड़ोसी राज्य आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल हैं। तमिल नाडु में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा तमिल है। तमिल नाडु के वर्तमान मुख्यमन्त्री एडाप्पडी पलानिस्वामी और राज्यपाल विद्यासागर राव हैं। .
नई!!: चन्द्रवाक्य और तमिल नाडु · और देखें »
दृग्गणित
दृग्गणित या दृक् गणित भारत में खगोलीय गणना की एक पद्धति है जिसका उपयोग अनेकों पारम्परिक खगोलशास्त्री, ज्योतिषी तथा पंचांग-निर्माता करते हैं।.
नई!!: चन्द्रवाक्य और दृग्गणित · और देखें »
परहितकरण
परहितकरण खगोलीय गणनाएँ करने की प्राचीन भारतीय पद्धति का नाम है। यह पद्धति मुख्यतः केरल और तमिलनाडु में प्रचलित थी। इसका आविष्कार केरल के खगोलशास्त्री हरिदत्त ने किया था। (683 ई)). नीलकण्ठ सोमयाजिन (1444–1544) ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ दृक्करण में इसका उल्लेख किया है कि उनके समय में 'परहित' की रचना किस प्रकार की गई थी। परहितकरण पद्धति के दो ग्रन्थ ज्ञात हैं - 'ग्रहचारनिबन्धन' तथा 'महामार्गनिबन्धन' किन्तु अब केवल ग्रहचारनिबन्धन ही प्राप्य है। 'परहित' का शाब्दिक अर्थ 'दूसरों की भलाई' है और वास्तव में 'परहितकरन' के निर्माण का उद्देश्य यही था कि खगोलीय गणनाओं को इतना आसान बना दिया जाय कि 'आम जनता' भी खगोलीय गणनाएँ करने में सक्षम हो जाय अतः 'सैद्धान्तिक' परिपाटी की कठिनाइयों को परहित-प्रणाली ने बहुत सरल बना दिया। इस प्रणाली ने आर्यभटीय में दी गयी गणना-चक्र को सरल बना दिया। हरिदत्त ने संख्याओं को निरूपित करने के लिए आर्यभट द्वारा विकसित 'कठिन' विधि के स्थान कटपयादि पद्धति को अपनाया। कटपयादि पद्धति बाद में केरलीय गणित में बहुत लोकप्रिय हुई। 'ग्रहचारनिबन्धनसंग्रह' (932 AD) नामक ग्रन्थ में 'परहित' विधि का विस्तार से वर्णन है। बाद में इन विधियों को भी परमेशवरन् ने १४८३ में रचित अपने 'दृग्गणित' (.
नई!!: चन्द्रवाक्य और परहितकरण · और देखें »
पंचांग
अल्फ़ोंसीन तालिकाएँ, जो १३वीं शताब्दी के बाद यूरोप की मानक पंचांग बन गई पंचांग (अंग्रेज़ी: ephemeris) ऐसी तालिका को कहते हैं जो विभिन्न समयों या तिथियों पर आकाश में खगोलीय वस्तुओं की दशा या स्थिति का ब्यौरा दे। खगोलशास्त्र और ज्योतिषी में विभिन्न पंचांगों का प्रयोग होता है। इतिहास में कई संस्कृतियों ने पंचांग बनाई हैं क्योंकि सूरज, चन्द्रमा, तारों, नक्षत्रों और तारामंडलों की दशाओं का उनके धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में गहरा महत्व होता था। सप्ताहों, महीनों और वर्षों का क्रम भी इन्ही पंचांगों पर आधारित होता था। उदाहरण के लिए रक्षा बंधन का त्यौहार श्रवण के महीने में पूर्णिमा (पूरे चंद की दशा) पर मनाया जाता था।, Sunil Sehgal, pp.
नई!!: चन्द्रवाक्य और पंचांग · और देखें »
संस्कृत भाषा
संस्कृत (संस्कृतम्) भारतीय उपमहाद्वीप की एक शास्त्रीय भाषा है। इसे देववाणी अथवा सुरभारती भी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत एक हिंद-आर्य भाषा हैं जो हिंद-यूरोपीय भाषा परिवार का एक शाखा हैं। आधुनिक भारतीय भाषाएँ जैसे, हिंदी, मराठी, सिन्धी, पंजाबी, नेपाली, आदि इसी से उत्पन्न हुई हैं। इन सभी भाषाओं में यूरोपीय बंजारों की रोमानी भाषा भी शामिल है। संस्कृत में वैदिक धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्मग्रंथ लिखे गये हैं। बौद्ध धर्म (विशेषकर महायान) तथा जैन मत के भी कई महत्त्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में लिखे गये हैं। आज भी हिंदू धर्म के अधिकतर यज्ञ और पूजा संस्कृत में ही होती हैं। .
नई!!: चन्द्रवाक्य और संस्कृत भाषा · और देखें »
संगमग्राम के माधव
संगमग्राम के माधव (सी. 1350 - सी. 1425) एक प्रसिद्ध केरल गणितज्ञ-खगोलज्ञ थे, ये भारत के केरल राज्य के कोचीन जिले के निकट स्थित एक कस्बे इरन्नलक्कुता से थे। इन्हें केरलीय गणित सम्प्रदाय (केरल स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथेमैटिक्स) का संस्थापक माना जाता है। वे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने अनेक अनंत श्रेणियों वाले निकटागमन का विकास किया था, जिसे "सीमा-परिवर्तन को अनंत तक ले जाने में प्राचीन गणित की अनंत पद्धति से आगे एक निर्णायक कदम" कहा जाता है। उनकी खोज ने वे रास्ते खोल दिए, जिन्हें आज गणितीय विश्लेषण (मैथेमैटिकल एनालिसि) के नाम से जाना जाता है। माधवन ने अनंत श्रेणियों, कलन (कैलकुलस), त्रिकोणमिति, ज्यामिति और बीजगणित के अध्ययन में अग्रणी योगदान किया। वे मध्य काल के महानतम गणितज्ञों-खगोलज्ञों में से एक थे। कुछ विद्वानों ने यह विचार भी दिया है कि माधव के कार्य केरल स्कूल के माध्यम से, जेसूट मिशनरियों और व्यापारियों द्वारा, जो उस समय कोच्ची के प्राचीन पत्तन के आसपास काफी सक्रिय रहते थे, यूरोप तक भी प्रसारित हुए हैं। जिसके परिणामस्वरूप, इसका प्रभाव विश्लेषण और कलन में हुए बाद के यूरोपीय विकास क्रम पर भी पड़ा होगा.
नई!!: चन्द्रवाक्य और संगमग्राम के माधव · और देखें »
वररुचि
वररुचि संस्कृत के अनेकानेक साहित्यिक, वैयाकरणिक एवं वैज्ञानिक ग्रन्थों से सम्बद्ध नाम है। प्राय: 'वररुचि' को 'कात्यायन' के साथ जोड़कर देखा जाता है जो पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों के वार्तिककार हैं। .
नई!!: चन्द्रवाक्य और वररुचि · और देखें »
वेण्वारोह
वेण्वारोह (.
नई!!: चन्द्रवाक्य और वेण्वारोह · और देखें »
कटपयादि संख्या
कटपयादि संख्या कर्नाटक संगीत में मेलापक राग की संख्या ज्ञात करने के काम आती है। इसके लिये राग के नाम के प्रथम दो सिलैबल्स के संगत कटपयादि संख्या निकालनी पड़ती है। .
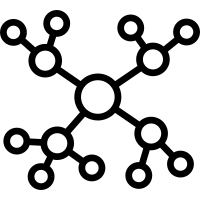
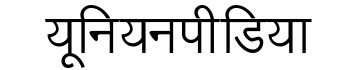

 ब्राउज़र की तुलना में तेजी से पहुँच!
ब्राउज़र की तुलना में तेजी से पहुँच!